RNI NO - 62112/95
ISSN - 2455-1171
औपनिवेशिक मानसिकता का साहित्य पर प्रभाव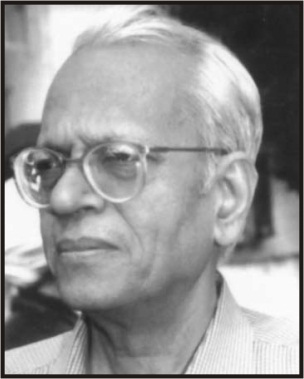
स्वतंत्र भारत में भोपाल में पहला लोकमंथन हुआ है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के अंतराल के बाद भारत का लोकमानस इस लोकमंथन के लिए तैयार हुआ है, यद्यपि ऐसा प्रयास देश के कई बुद्धिजीवी अपने-अपने स्तर पर करते रहे हैं और अपने समय के देश-काल को अपनी देशीय दृष्टि, अपने भारतीय दृष्टिकोण से देखते रहे हैं। यहाँ तक कि भारतेतर देशों में रहने वाले भारतीय विद्वानों ने भारत को भारत की दृष्टि से देखने-समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। इधर राजीव मल्होत्रा की पुस्तक ‘बीइंग डिफरेंट’, जो हिंदी में ‘विभिन्नता’ के नाम से प्रकाशित हुई है, काफी चर्चा में है और पाश्चात्य सार्वभौमिकता को चुनौती देनेवाली यह पुस्तक हमारे विचार के केंद्र में हो सकती है। भारत में ऐसे लोकमंथन की परंपरा रही है। समुद्र मंथन, शास्त्रार्थ और संवाद तथा कुंभ मेलों में विद्वानों का विचार-विमर्श ऐसे ही मंथन की लंबी परंपरा है। असल में लोकमंथन लोक जागृति का परिणाम है। मध्यकाल में मुसलिम आक्रमणकारियों एवं क्रूर शासकों के विरुद्ध संत कवियों ने एक राष्ट्रव्यापी लोक जागरण उत्पन्न किया। भारत में इसलाम का आक्रमण एक विचित्र चुनौती थी, जिसका सामना भक्ति आंदोलन ने किया। अपनी काव्य-रचना से विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया तथा हिंदू धर्म-संस्कृति को बचाकर रखा। इससे भी भयंकर स्थिति अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी में उत्पन्न हुई, जब व्यापारी अंग्रेजों ने देश पर कब्जा करके उसे गुलाम बनाया और अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का एक अंग बना लिया। मुसलिम आक्रमणकारियों के पास बौद्धिक संपदा के रूप में केवल ‘कुरान’ थी, और वे उसे ही ज्ञान की अंतिम कसौटी मानते थे, अतः उन्होंने नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया और शक्ति से हिंदुस्तान को धर्मांतरित करने का प्रयत्न किया, परंतु अंग्रेजों में शक्ति और व्यापारिक बुद्धि तो थी ही, अपने धर्म, संस्कृति, ज्ञान, जीवन-शैली आदि में सर्वश्रेष्ठ होने तथा भारत जैसे उपनिवेश को हीनतम समझने और समझाने का तीव्र अहंकार भी था। इस पश्चिमी अहंकार को स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद आदि ने चुनौती दी। गांधी ने पश्चिमी सभ्यता को ‘राक्षसी सभ्यता’ कहा था और अंग्रेज बने हिंदुस्तानियों की तीव्र भर्त्सना की थी कि इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों में जाकर हिंदू धर्म-संस्कृति की श्रेष्ठता की स्थापना की और उन भारतीयों को धिक्कारा, जो अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हम नीच हैं, हम बहुत क्षुद्र हैं, हमारा सबकुछ खराब है और आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट मत है कि भारत में अपना बल एवं सार है और अब भी हमारे पास जगत् के सभ्यता भंडार में जोड़ने के लिए कुछ है और इसीलिए हम बचे हैं। लाला लाजपतराय ने अपनी पुस्तक ‘यंग इंडिया’ में यूरोप यात्रा के अनुभव लिखे हैं। वे लिखते हैं कि यूरोप के उच्च शिक्षकों को भारत के बारे में बहुत कम ज्ञान है और उन्हें ईसाई मिशनरियों, अंग्रेज अफसरों एवं लेखकों आदि से जो कुछ ज्ञात होता है, वे उसे ही सत्य मानते हैं। भारत आनेवाले यूरोपियन मानते हैं कि भारत पत्थर और साँपों को पूजता है, यहाँ सभ्य-सुगठित सरकार कभी नहीं रही और अंग्रेजों ने पहली बार स्थायी सरकार दी और अंग्रेजों के जाने पर भारत टुकड़ों में बँट जाएगा और भारतीय जानवरों की तरह हैं और अंग्रेज ही उनका उद्धार कर सकते हैं। भारत कोई राष्ट्र नहीं था, अंग्रेजों ने उसे राष्ट्र बनाया और भारत को गुलाम बनाने के औचित्य के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत गढ़ा। बाद में भारतीय कम्युनिस्टों ने हिंदुत्व का विरोध करने के लिए इस थीसिस से सहायता ली। लार्ड मैकाले के शिक्षा-दर्शन तथा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार में भी ईसाई मिशनरियों के समान ही भारत को ईसाई देश में बदलने की भी धारणा॒थी। लार्ड मैकाले का मत था कि अंग्रेजी शिक्षा से एक ओर ब्रिटेन का व्यापार बढ़ेगा और दूसरी ओर भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा हो जाएगा, जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हो, परंतु रुचि, विचार और दिमाग से वह अंग्रेजी और अंग्रेजों का गुलाम ही बना रहेगा। ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य भी इससे भिन्न नहीं था। उस समय अंग्रेजी शिक्षा और ईसाइयत एक-दूसरे के पर्याय बन गए थे। मैकाले ने अपनी माँ को लिखा था कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ के तीस साल के अंदर बंगाल में एक भी मूर्तिपूजक नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने व्यापार करते हुए एक बार भारत को जीता था, अब वह शिक्षा और धर्म के हथियार से भारत को संपूर्ण रूप से जीतना चाहते थे। खेदजनक यह है कि इसमें अंग्रेजी पढे़-लिखे कुछ भारतीय अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। मैक्समूलर ने उस सच्चाई को उद्घाटित करते हुए २३ नवंबर, १८९८ को सर हेनरी ऑकलैंड को लिखा था—‘‘यदि हमें राजा राममोहन राय अथवा केशवचंद्र सेन जैसे व्यक्ति पुनः भारत में मिल जाएँ और एक ईसाई धर्म का ज्ञाता अर्क विशप मिल जाए तो भारत ईसाई बन जाएगा।’’ उन्नीसवीं शताब्दी में और १८५७ की क्रांति के बाद औपनिवेशिक दासता पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी और पुनर्जागरण की लहरें भी उठने लगी थीं। संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करके भारत को जानने और समझने और उसकी यूरोपीय दृष्टि से व्याख्या करने की प्रवृत्ति भी बन चुकी थी और इधर भारत की आत्मा को आहत एवं छिन्न-भिन्न करने के प्रयास चल रहे थे। भारत के मानस को पराजित करने और अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने तथा भारत को ‘इंडिया’ में बदलने के दौर में देश के कुछ अंग्रेजी शिक्षित युवकों ने औपनिवेशिक दासता को चुनौती के रूप में ग्रहण किया और देश में एक सांस्कृतिक जागरण का युग शुरू हुआ। इससे भारत के कुछ शिक्षित लोग, धर्माचार्य, राजनेता और साहित्यकार प्रेरित होकर भारत की खोज एवं स्वत्व की पहचान की ओर प्रवृत्त हुए। इसमें साहित्य ने अपनी आवाज बुलंद की और लगभग सभी भाषाओं में भारतीय चेतना एवं अस्मिता को पारिभाषित करके जनता के सम्मुख रखा जाने लगा। हिंदी में इसका आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है, जिसमें उन्होंने अपने स्वत्व, स्वभाषा और स्वसंस्कृति से ओतप्रोत रचनाएँ प्रस्तुत कीं। उस युग में हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी को अपने साहित्य का आधार बनानेवाले अनेक लेखक दिखाई देते हैं। इनमें मैथिलीशरण गुप्त का योगदान सर्वोपरि है। उनकी चिंता यह थी कि भारतीय क्या थे, क्या हैं तथा भविष्य में क्या होंगे? उन्होंने अपने भारतीय चिंतन एवं श्रेष्ठ होने के भाव को पौराणिक कथानकों के साथ प्रस्तुत किया और हिंदू धर्म-संस्कृति की उच्चता की स्थापना की। यह एक प्रकार से साहित्य में हिंदू धर्म-संस्कृति तथा परंपरागत जीवन-मूल्यों के पुनरुत्थान का युग था, जो औपनिवेशिक दासता के दमनकारी परिवेश में पुनः जीवंत होने का प्रयास कर रहा था। उस युग की अधिकांश पत्रिकाओं का उद्देश्य दासता के विरुद्ध स्वाधीन, बौद्धिक तथा जीवंत भारत की सृष्टि करना था। दासता के विरुद्ध स्वराज की कल्पना की गई और बंग-भंग, खुदीराम बोस की फाँसी आदि घटनाओं के परिदृश्य के बीच हिंदी-उर्दू के महान् कथाकार प्रेमचंद ने औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध भारत की सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठता को स्थापित किया। प्रेमचंद ने अपने सन् १९१२ के लेख ‘हिंदू सभ्यता और लोक-हित’ में स्थापित किया कि ईसाई धर्म के जन्म से हजारों वर्ष पहले हिंदुस्तान ने शिक्षा, उपचार, पशु-प्रेम, उदारता आदि में उच्चता प्राप्त कर ली थी। उनका कथन है कि भौतिकता पश्चिमी सभ्यता की आत्मा है और व्यापार, स्वार्थ, लाभ आदि उसके अंग हैं और हिंदू सभ्यता नैतिकता, आध्यात्मिकता, दानशीलता, आत्मोत्सर्ग एवं चारित्रिक साहस पर टिकी है। योरोपियन कौमें जिन दूसरी कौम को नीची दृष्टि से देखती हैं, उनकी प्राचीन महत्ता को स्वीकार नहीं करतीं। प्रेमचंद ने अपने कई लेखों में हिंदू तथा ईसाई संस्कृति तथा पूर्व एवं पश्चिम का तुलनात्मक विवेचन किया है और हिंदू संस्कृति की श्रेष्ठता को ही स्थापित किया है और भारत पर औपनिवेशिक दासता के पड़नेवाले प्रभावों को अपने लेखों तथा कहानियों एवं उपन्यासों में रेखांकित किया है। एक साहित्यकार के रूप में वे भारत की मानसिक दासता से पीडि़त हैं और मानसिक दासता लेख में इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रेमचंद का यह लेख भारतीयों की मानसिक दासता तथा अंग्रेजों से स्वयं को हीन समझने की प्रवृत्ति एवं हर क्षेत्र में नकल करने की आदत से जातीय संस्कृति के लुप्त हो जाने की संभावना की ओर ध्यान आकर्षित करता है। वे लिखते हैं कि पश्चिमवालों को शक्तिशाली देखकर हम मान लेते हैं कि हममें सिर से पाँव तक दोष ही दोष हैं और उनमें सिर से पाँव तक गुण ही गुण। प्रेमचंद इस लेख में भाषा, वेशभूषा, आचार-व्यवहार, जीवन-मूल्य आदि में मानसिक दासता का विवेचन करते हैं और रोषपूर्ण शब्दों में लिखते हैं कि हम भाषा, वेशभूषा आदि में अपनी दासता के कलंक को दिखाते फिरते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं, उस पर अभिमान करते हैं, मानो वह नेकनामी का तमगा हो या हमारी कीर्ति की ध्वजा। वाह री दासता! तेरी बलिहारी है। हम मानसिक पराजय के कारण पश्चिमी चीजों की आँख बंद करके नकल करते हैं, लेकिन यह भी ठीक है कि हमारी सभ्यता में भी रोग हैं, मगर उसकी दवा यूरोपीय सभ्यता की अंध-भक्ति नहीं है। उसकी दवा हमें अपनी संस्कृति में ही खोजनी होगी। हमें यह समझना होगा कि यह राजनीतिक परिस्थिति नहीं रहेगी, परंतु इस परिस्थिति में यदि हमने अपना अस्तित्व, धर्म और संस्कृति खो दी तो हमारा अंत हो जाएगा। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में अनेक ऐसे हिंदुस्तानी पात्रों की सृष्टि की है, जो काले अंग्रेज बनकर अपनी संस्कृति के शत्रु और अंग्रेजी सभ्यता के अनुयायी बन गए हैं, परंतु वे उसका दुखद परिणाम दिखाते हुए उनका मानसिक कायाकल्प करते हैं। इसके लिए वे मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा को दोषी ठहराते हैं। वे अपने एक उपन्यास में अंग्रेजी विश्वविद्यालयों को ग्रैजुएट उत्पादित करनेवाले कारखाने बताते हैं और ऐसे शिक्षितों की मानसिक दासता का चित्रण करते हैं। मैं यहाँ विस्तार भय से बचने के लिए उनकी केवल तीन-चार कहानियों की चर्चा करूँगा। उनकी हिंदी में प्रकाशित पहली कहानी है ‘परीक्षा’, जो सन् १९१४ में प्रकाशित हुई थी। कहानी में देवगढ़ रियासत के लिए एक दीवान चुनने का प्रसंग है। दीवान के लिए अनेक ग्रैजुएट युवक उम्मीदवार हैं, परंतु अधिकांश में विपत्ति में पड़े किसान की मदद करने और उसकी व्यथा समझने का भाव नहीं है। ये सभी मानवीय गुणों से शून्य हैं, अतः एक ऐसे युवक का चयन होता है, जो पैर में चोट लगने पर भी कीचड़ में घुसकर किसान की फँसी गाड़ी को निकालता है। इस प्रकार प्रेमचंद अंग्रेजी पढ़े-लिखे युवकों की परीक्षा लेते हैं, जो मानवीयता की परीक्षा में असफल होते हैं। ‘लाल फीता’ (१९२१) उनकी ऐसी दूसरी कहानी है, जिसमें एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट यह मानता है कि अंग्रेजी राज्य सत्य और न्याय पर टिका है, उनके शासन में शिक्षा एवं व्यापार की उन्नति हुई है और अंग्रेज दीनों तथा असहायों के रक्षक हैं, परंतु वे सरकारी हुक्म के अनुसार जाति के सेवकों तथा हितैषियों से शत्रुवत् व्यवहार को तैयार नहीं होते और विजातीय शासक के देशद्रोही आदेश के विरुद्ध सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। इसके लिए वे अंग्रेजी शिक्षा को दोषी ठहराते हैं जो मनुष्य को विलास प्रेमी बनाती है। तीसरी कहानी ‘बड़े बाबू’ है, जिसमें एक ग्रैजुएट सरकारी नौकरी पाने के लिए मुखबिरी तथा वेश्याओं की दलाली तक करने को तैयार है। एक और कहानी है ‘रोशनी’, इसका नायक इंग्लैंड से आई.सी.एस. (आई.ए.एस.) बनकर आता है तो उसकी नियुक्ति पहाड़ी प्रदेश में होती है। यह हिंदुस्तानी अफसर मानता है कि पश्चिम शिक्षा में पथ प्रदर्शक है और नन्हा सा इंग्लैंड आधी दुनिया पर हावी है, जबकि हिंदुस्तान में अधनंगे फकीरों की महत्ता है और पेड़ एवं पत्थर की पूजा होती है तथा जिंदगी के प्रत्येक विभाग में धर्म घुसा हुआ है, लेकिन जब यह अफसर तूफान में घिर जाता है तो एक ग्रामीण स्त्री उसका मार्गदर्शन करती है और इस प्रकार उसकी अंग्रेजियत भारत के प्रति सेवाभाव में बदल जाती है। प्रेमचंद ने लिखा है कि हिंदुस्तानी साहबों की एक बिरादरी हो गई है उनका रहन-सहन, चाल-ढाल, पहनावा, बर्ताव सब अंग्रेजों जैसा है। देश में यह नई उपज है, जो अंग्रेजी साहब करता है, वही हमारा हिंदुस्तानी साहब करता है। अंग्रेजियत ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है। गाँव की एक औरत उसके इस भ्रम को तोड़ती है और उसे जिंदगी की सच्ची रोशनी देती है। उनकी पाँचवीं कहानी है ‘यही मेरी मातृभूमि है’, जो बंग-भंग के बाद सन् १९०८ में छपी थी। यह कहानी भारतीय समाज पर औपनिवेशिक दासता के प्रभाव को प्रस्तुत करती है और देश-विरोधी प्रवृत्तियों में ठेठ देशज समाधान को चुनती है। कहानी में एक भारतीय अमेरिका में सुख-समृद्धि का जीवन जीने के साठ वर्ष बाद भारत लौटता है कि अंतिम समय में अपनी प्यारी भारत जननी के दर्शन कर सकूँ और अपनी मातृभूमि का रज-कण बन सकूँ। वह अमेरिका में बराबर महसूस करता है कि यह मेरा देश नहीं है और मैं इस देश का नहीं हूँ। वह बंबई (मुंबई) जहाज से उतरता है तो उसे कोट-पतलून पहने टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलते मल्लाह मिलते हैं और अंग्रेजी दुकान, ट्राम और मोटरगाडि़याँ दिखाई देती हैं। वह रेल में बैठकर अपने गाँव जाता है तो खूब रोता है, क्योंकि यह वह देश नहीं है, जिसके दर्शनों की इच्छा से वह आया है। वह कहता है कि यह अमरीका या इंग्लैंड है, मगर प्यारा भारत नहीं है। वह जब गाँव पहुँचता है, तब वहाँ भी सबकुछ बदल गया है। उसका घर टूट गया है, लँगोटिया यार मर गए हैं, बरगद के पास पुलिस थाना है, चौपाल में डाकखाना है, धर्मशाला दुराचार का अड्डा है तथा परदेसी यात्री को रात में ठहराने को कोई तैयार नहीं है। वह मानता है कि यह यूरोप है, अमरीका है, मगर मेरा प्यारा भारत नहीं है। वह अब स्वयं को देशविहीन मानता है कि तभी भोर में कुछ स्त्रियों को गंगा-स्नान करने जाते देखता है, जो ‘हमारे प्रभु, अवगुन चित न धरो’ गाती जा रही हैं। वह इसमें देश का राग और मातृभूमि का स्वर पाता है। वह देखता है कि कुछ लोग शिव-शिव, हर-हर, गंगे-गंगे, नारायण-नारायण आदि बोलते जा रहे हैं। वह उनके पीछे पतित-पावनी गंगा के किनारे पहुँचता है और कोट-पतलून उतारकर फेंकता है तथा गंगा की गोद में कूद पड़ता है और कह उठता है, ‘‘हाँ, हाँ, यही मेरा प्यारा देश है, यही मेरी मातृभूमि है, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ भारत है और इसी के दर्शनों की मेरी उत्कट इच्छा थी तथा इसी की पवित्र धूलि के कण बनने की मेरी प्रबल अभिलाषा है।’’ वह गंगा के किनारे छोटी सी झोंपड़ी बनवाकर रहता है, नित्य गंगा स्नान करता है और रामनाम जपता है और चाहता है कि मरने पर उसकी अस्थियाँ गंगा माता की लहरों की भेंट हों। इस प्रकार प्रेमचंद औपनिवेशिक दासता में भारतीय जीवन में विजातीय ढाँचे का उद्घाटन करते हैं, जो हमारे देसी संस्कारों, विश्वासों तथा जीवन-शैली को विस्थापित करके विदेशी संस्कृति को स्थापित कर रहा है। पश्चिमी शिक्षा का फैलता तंत्र हमारे तन-मन और आस्थाओं को तेजी से बदलता है और सीधे ही भारतीय संस्कृति के मूल्यों एवं प्रतिमानों से टक्कर होती है। प्रेमचंद इन संस्कृतियों के संघर्ष में भारतीय मूल्यों की रक्षा करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि मैं अपने साहित्य में भारतीय आत्मा की रक्षा करना चाहता हूँ। औपनिवेशिक दासता के उस कू्रर काल में प्रेमचंद की कथाएँ स्वाधीनता संग्राम को बल प्रदान करती हैं और स्वराज की स्थापना में स्व-संस्कृति, स्व-चिंतन तथा स्व-भाषा का महत् स्वप्न बना रहता है, यद्यपि यह दुर्भाग्य ही था कि स्वतंत्र भारत की सत्ता देसी अंग्रेजों के हाथ में आ गई और भारतीय आत्मा की रक्षा का स्वप्न गायब हो गया। और अंत में, हम स्वतंत्र भारत में फिर भारत की खोज और भारतीय आत्मा की पहचान की ओर लौट रहे हैं, यह सोचकर कि भारतभूमि पर देसी पौधा ही फल-फूल सकता है। हमें ‘इंडिया’ को ‘भारत’ का रूप देना ही होगा, क्योंकि भारतीय लोकमानस अपने भारतीय स्वत्व एवं राष्ट्र-बोध के साथ ही विकासमान हो सकता है। आज भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति तथा भूमंडलीकरण का दवाब पहले से बढ़ गया है और देसी अस्मिता एवं संस्कृति के अस्तित्व पर संकट आ गया है। इस राष्ट्रीय संकट के समय लोक-मंथन से ही हमें अमृत और विष का पता चलेगा। हमारी औपनिवेशिक दासता खत्म हो गई है, परंतु एक नई सांस्कृतिक दासता का धुआँ हमें घेरता जा रहा है। हमें इसका हल ढूँढ़ना ही होगा और मुझे आशा है कि यह लोकमंथन एक नई राष्ट्रीय-सांस्कृतिक जागृति के युग को प्रशस्त करेगा। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, वर्तमान सरकार ने आत्मचेतना एवं आत्मनिर्भरता का द्वार खोल दिया है, बस हमें वेद के अनुसार साथ-साथ चलकर, साथ-साथ सोचकर इस भारतीय लक्ष्य को पूरा करना है। यह लोकमंथन इसी का संकल्प लेकर पूरा होना चाहिए। ए/९८, अशोक विहार, फेज प्रथम, दिल्ली-११००५२ दूरभाष : ९८११०५२४६९ |
अप्रैल 2024 |













